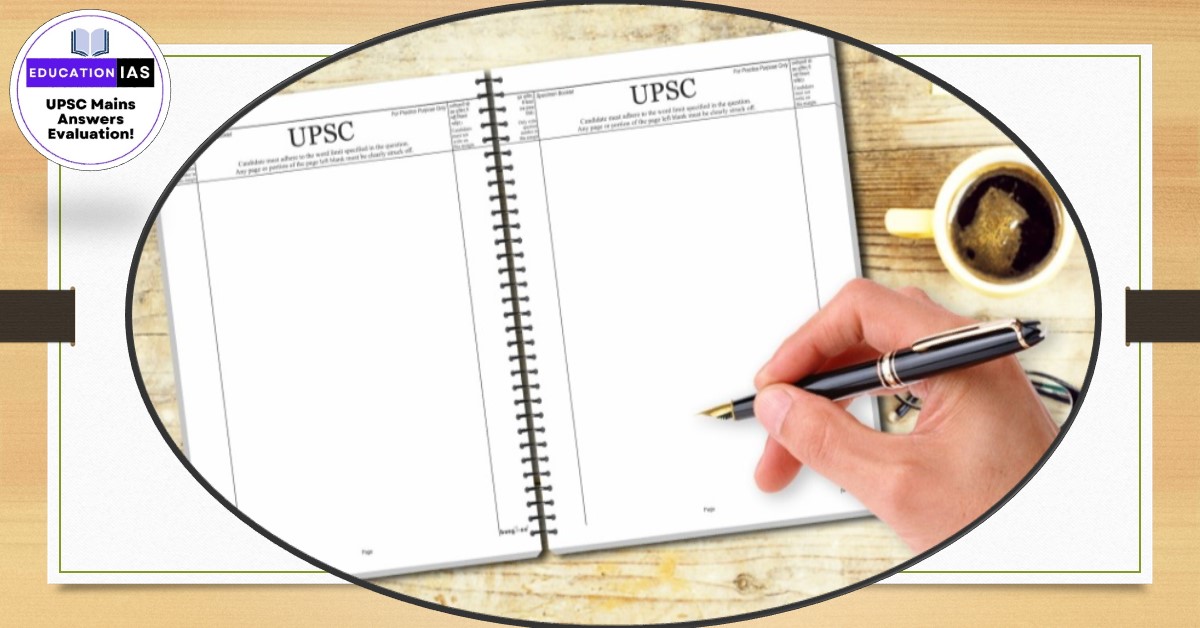| बाह्य दबाव और औपनिवेशिक विरोध के साथ-साथ घरेलू दबाव ने यूरोपीय शक्तियों को उपनिवेशों पर अपना दावा छोड़ने के लिए विवश किया। सविस्तार वर्णन कीजिए। |
दृष्टिकोण:
(i) द्वितीय विश्व युद्धोत्तर काल में औपनिवेशीकरण की स्थिति के बारे में संक्षिप्त वर्णन करते हुए उत्तर आरंभ कीजिए।
(ii) उन बाह्य दबावों और औपनिवेशिक विरोधों के साथ-साथ घरेलू दबावों पर प्रकाश डालिए जिसके कारण यूरोपीय शक्तियां उपनिवेशों पर अपना दावा छोड़ने के लिए विवश हो गई थीं।
(iii) संक्षिप्त निष्कर्ष प्रस्तुत कीजिए।
परिचय:
1945 में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद भी यूरोपीय देशों ने विश्व के शेष विशाल क्षेत्र, विशेष रूप से एशिया और अफ्रीका में अपना स्वामित्व बनाए रखा। हालांकि, इनमें से अधिकांश औपनिवेशिक क्षेत्र 1975 तक स्वतंत्र हो गए थे।
विभिन्न कारकों के परिणामस्वरूप यूरोपीय शक्तियां उपनिवेशों पर अपना दावा छोड़ने पर विवश हो गई; जैसे-
1. घरेलू दबाव
यूरोपीय देशों के भीतर उपनिवेशवाद के विरुद्ध विरोध आरंभ हो गए थे। उदाहरण के लिए, सामान्य तौर पर लेबर पार्टी उपनिवेशों के आर्थिक और राजनीतिक विकास का समर्थन तथा उनके शोषण का विरोध करती थी। वास्तव में 1945 के चुनाव में भारत की स्वतंत्रता, लेबर पार्टी का एक चुनावी वादा था।
इसके अतिरिक्त, युद्ध ने यूरोपीय राज्यों को कमजोर कर दिया और सैन्य या आर्थिक रूप से अब वे इतने मजबूत नहीं थे कि अपने सुदूरवर्ती उपनिवेशों पर अधिकार बनाए रख सकें। इस प्रकार, रखरखाव की अत्यधिक लागत और उपनिवेशों से मिलने वाले कम लाभ ने उन्हें वि-उपनिवेशीकरण की ओर बढ़ने के लिए विवश कर दिया।
2. बाह्य दबाव
ब्रिटिश साम्राज्य का एक भूतपूर्व उपनिवेश संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) साम्राज्यवाद का कट्टर विरोधी था। राष्ट्रपति रूजवेल्ट और उनके उत्तराधिकारी दूमैन ने ब्रिटिश सरकार पर भारत को शीघ्र स्वतंत्र करने हेतु दबाव बनाया।
USA ने यूरोपीय शक्तियों पर उपनिवेशों की स्वतंत्रता हेतु इसलिए भी दबाव बनाया क्योंकि एशिया और अफ्रीका में यूरोपीय उपनिवेशों को स्वतंत्रता मिलने में होने वाले विलंब से इन क्षेत्रों में साम्यवाद के प्रसार की संभावना थी।
इसके अतिरिक्त, USA ने नव-स्वतंत्र राष्ट्रों को संभावित बाजारों के रूप में देखा। USA के अनुसार, साम्राज्यवाद के रूप में संरक्षित बाजारों से ब्रिटिश और अन्य यूरोपीय लोगों को अनुचित लाभ मिला है।
संयुक्त राष्ट्र चार्टर के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र संघ ने आत्मनिर्णय और मूलभूत मानवाधिकारों पर बल दिया था। इससे औपनिवेशिक शक्तियों पर उपनिवेशवाद को समाप्त करने का दबाव उत्पन्न हुआ। संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) द्वारा 1960 में वि-उपनिवेशीकरण पर एक घोषणा (Declaration on Decolonisation) को भी अंगीकृत किया गया था।
सोवियत संघ ने भी उपनिवेशवाद का विरोध किया और निरंतर साम्राज्यवाद की निंदा की।
3. औपनिवेशिक विरोध
औपनिवेशिक शक्तियां उपनिवेशों के भीतर राष्ट्रवादी दबाव में वृद्धि के कारण भी अपने अधीनस्थ क्षेत्रों को त्यागने के लिए भी विवश हो गई थीं। इसके कारण उनके पास कोई अन्य विकल्प नहीं बचा था। यूरोप के कई उपनिवेशों, विशेष रूप से एशिया में, राष्ट्रवादी आंदोलन चल रहे थे।
भारत में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 से ही ब्रिटिश शासन के विरुद्ध आंदोलन कर रही थी। इसके अतिरिक्त, दक्षिण-पूर्व एशिया में वियतनामी राष्ट्रवादियों (Vietnamese nationalists) ने 1920 के दशक के दौरान फ्रांसीसी शासन के विरुद्ध अभियान प्रारंभ कर दिया था। ‘भारत छोड़ो’ और ‘शाही भारतीय नौसेना में विद्रोह’ जैसे आंदोलनों के कारण साम्राज्यवादियों के लिए उपनिवेशों पर अपने शासन को बनाए रखना असंभव हो गया था।
द्वितीय विश्व युद्ध ने कई प्रकार से राष्ट्रवादी आंदोलनों को व्यापक प्रोत्साहन दिया; जैसे-
इस विश्व युद्ध ने यूरोपीय अपराजेयता की धारणा को समाप्त कर दिया। युद्ध के आरंभिक दौर में जापान की सफलता से यह सिद्ध हो गया कि गैर-यूरोपीय लोग भी यूरोपीय सेनाओं को पराजित कर सकते हैं।
युद्ध में शामिल होने के परिणामस्वरूप एशियाई और अफ्रीकी लोग सामाजिक एवं राजनीतिक मामलों के बारे में अधिक जागरूक हो गए थे। इनमें से अधिकांश लोग पहले कभी अपने देश से बाहर नहीं गए थे। उन्होंने जब अपनी आदिम जीवन स्थितियों और सशस्त्र बलों के सदस्यों के रूप में भी अनुभव की गई अपेक्षाकृत आरामदायक स्थितियों के बीच अंतर को देखा तब वे व्याकुल हो उठे।
निष्कर्ष:
उपर्युक्त सभी कारकों ने विश्व भर के राष्ट्रवादियों को अपने अभियानों को और तेज़ करने के लिए प्रोत्साहित किया। इसके अतिरिक्त, विदेश और आर्थिक नीति के क्षेत्र में औपनिवेशिक भूमिकाओं को ‘आधुनिक’ लक्ष्यों के साथ असंगत के रूप में भी देखा जाने लगा।