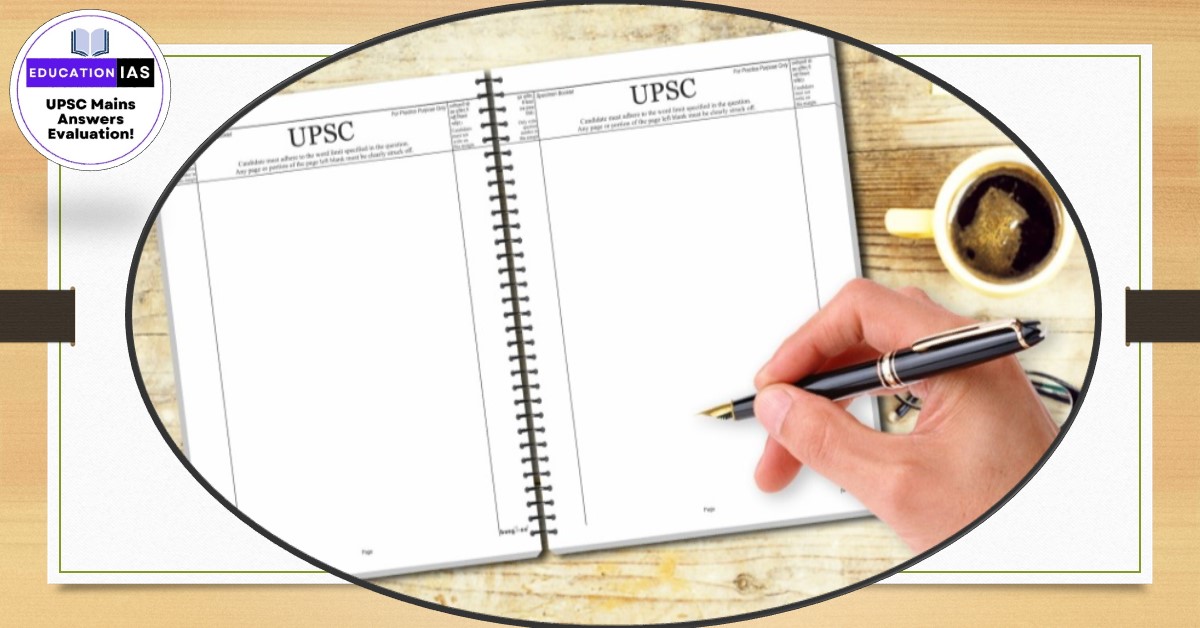| स्वातंत्र्योत्तर भारत में, जनजातीय लोगों की समृद्ध सामाजिक और सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण, सरकार की जनजातीय एकीकरण की नीति के केंद्र में रहा है। विवेचना कीजिए। |
दृष्टिकोण:
(i) स्वतंत्रता के बाद जनजातीय लोगों की स्थिति के बारे में टिप्पणी करते हुए उत्तर आरंभ कीजिए।
(ii) जनजातीय लोगों के लिए सरकार की नीति पर चर्चा कीजिए।
(iii) तदनुसार निष्कर्ष प्रस्तुत कीजिए।
परिचय:
स्वातंत्र्योत्तर भारत में जनजातीय लोगों को मुख्यधारा में शामिल करने का कार्य काफी कठिन था। खासतौर पर इसलिए क्योंकि जनजातीय लोग देश के विभिन्न भागों में अलग-अलग भौगोलिक और सामाजिक परिस्थितियों में रह रहे थे। 1971 की जनगणना के अनुसार, भारत में 400 से अधिक जनजातीय समुदाय थे। ये भारतीय जनसंख्या का लगभग 6.9 प्रतिशत थे।
सरकार ने जनजातीय लोगों की विशिष्ट पहचान और संस्कृति को अक्षुण्ण रखते हुए उन्हें भारतीय समाज में एकीकृत करने की नीति निम्नलिखित तरीके से अपनाई:
(i) परंपरागत प्रथाओं को संरक्षित करना और उनको बढ़ावा देनाः
यह परिकल्पना की गई थी कि जनजातीय लोगों को अपनी बुद्धि और चेतना के अनुरूप विकास करने देना चाहिए। उन पर कोई बाह्य पद्धति थोपी नहीं जानी चाहिए।
इसी बात को ध्यान में रखते हुए पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार) अधिनियम या पेसा अधिनियम, 1996 लागू किया गया था। इसका उद्देश्य ग्राम सभा की सक्रिय भागीदारी के साथ-साथ जनजातीय आबादी को बाहरी शोषण से संरक्षण प्रदान करना था।
(ii) भूमि और वन अधिकारों का संरक्षणः
राज्य द्वारा भूमि और वनों के संबंध में जनजातीय अधिकारों का संरक्षण करने और बाहरी लोगों को जनजातीय भूमि पर कब्जा करने से रोकने के प्रयास किए गए। इन प्रयासों का उद्देश्य जनजातीय क्षेत्रों में बाजार अर्थव्यवस्था के हस्तक्षेप को सख्ती से नियंत्रित और विनियमित करना था।
इसी बात को ध्यान में रखते हुए अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 लाया गया। इसका उद्देश्य भारत में जनजातीय लोगों के भूमि और वन संबंधी अधिकारों का संरक्षण करना था।
(iii) भाषाई पहचान को संरक्षित करनाः
इसके लिए यह आवश्यक था कि जनजातीय भाषाओं के संरक्षण एवं विकास को प्रोत्साहित किया जाए तथा उन परिस्थितियों को संभव बनाया जाए जिनमें उनका विकास हो सके। सरकार जनजातीय अनुसंधान संस्थान को विभिन्न अनुसंधान और दस्तावेज़ीकरण संबंधी गतिविधियों के लिए सहायता प्रदान करती है। इसमें जनजातीय भाषाओं, बोलियों आदि के दस्तावेज़ीकरण जैसे कार्यक्रम शामिल हैं।
(iv) प्रशासनिक रक्षोपायः
स्वशासन भारत में जनजातीय प्रशासन की एक मुख्य विशेषता रही है। इसे संविधान की पांचवीं और छठी अनुसूची के तहत जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए विशेष प्रावधानों के माध्यम से सुनिश्चित किया गया है।
(v) संधारणीय आजीविका सुनिश्चित करनाः
लघु वन उपज (MFP) के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) जैसी योजनाओं को लघु वन उपज एकत्रित करने वाले लोगों की आजीविका में सुधार के लिए एक सामाजिक सुरक्षा उपाय के रूप में तैयार किया गया था। इसका उद्देश्य उनके द्वारा एकत्रित MFP के लिए उन्हें उचित मूल्य प्रदान करना था।
निष्कर्ष
संवैधानिक सुरक्षा उपायों तथा केंद्र एवं राज्य सरकारों के प्रयासों के बावजूद जनजातीय लोगों की प्रगति और कल्याण बहुत धीमा और निराशाजनक रहा है। जनजातीय लोग अभी भी गरीब, कर्जदार, भूमिहीन और प्रायः बेरोजगार बने हुए हैं।
यह समस्या मुख्य रूप से अच्छे एवं दृढ़ इच्छाशक्ति वाले उपायों के कमजोर कार्यान्वयन के कारण बनी हुई है। साथ ही, कई बार केंद्र एवं राज्य सरकार की जनजातीय नीतियों में भी काफी अंतर देखा जाता है।
इन चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए अनुसूचित जनजातियों की विशिष्ट संस्कृति एवं जीवन शैली को प्रभावित किए बिना उनके सर्वांगीण विकास के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण के जरिए उन्हें समाज की मुख्यधारा में लाना आवश्यक है।