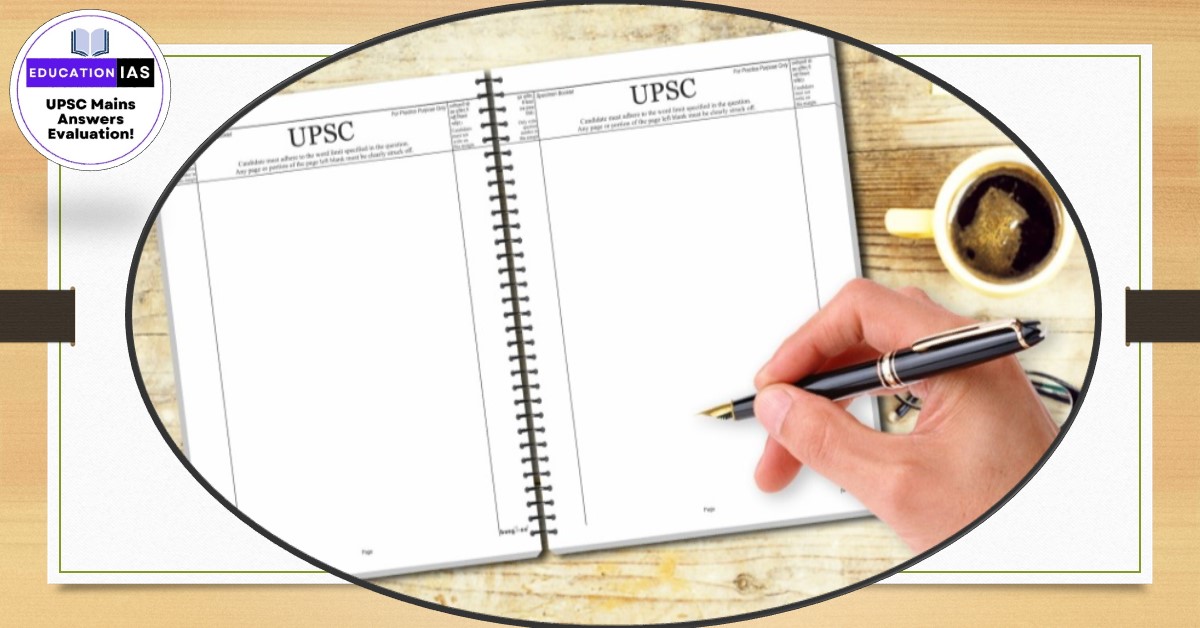| भारत में मंदिर स्थापत्य कला का एक प्रमुख चरण 11वीं से 14वीं शताब्दी ईसवी के होयसल राजवंश से जुड़ा हुआ है। उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। |
दृष्टिकोण:
(i) होयसल स्थापत्य कला का संक्षेप में वर्णन करते हुए उत्तर प्रारंभ कीजिए।
(ii) विशिष्ट उदाहरणों के साथ होयसल मंदिर स्थापत्य कला की विशिष्ट विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए चर्चा कीजिए कि होयसल राजवंश की मंदिर स्थापत्य कला एक विशिष्ट चरण क्यों है।
(iii) तदनुसार निष्कर्ष प्रस्तुत कीजिए।
परिचय:
भारत में, मंदिर स्थापत्य कला की दो श्रेणियां पाई जाती हैं- एक उत्तर भारत की नागर शैली और दूसरी दक्षिण भारत की द्रविड़ शैली।
कालांतर में, नागर और द्रविड़ शैलियों की कुछ चयनित विशेषताओं को मिलाते हुए वेसर शैली नामक एक स्वतंत्र शैली का विकास किया गया।
11वीं से 14वीं शताब्दी ईस्वी तक शासन करने वाले कर्नाटक के होयसल राजवंश ने हलेबिड, बेलूर, सोमनाथपुर और दक्षिणी दक्कन के अन्य क्षेत्रों में सैकड़ों मंदिरों का निर्माण वेसर शैली में करवाया था।
होयसल राजवंश ने भारत में मंदिर स्थापत्य कला के एक विशिष्ट चरण का निर्माण किया है; जैसे-
1. अद्वितीय समन्वयवाद के दो उदाहरण:
मंदिर स्थापत्य कला में नागर और द्रविड़ शैलियों का एकीकरण।
धार्मिक बहुलवाद अथवा धार्मिक सहिष्णुता की प्रत्यक्ष स्वीकृति। उदाहरण के लिए, 12वीं शताब्दी के आरंभ में विष्णुवर्धन के शासनकाल के दौरान हलेबिड मंदिरों का निर्माण किया जाना। इनमें शिव को समर्पित होयसलेश्वर मंदिर के साथ-साथ तीन बड़ी जैन बसदियों का भी निर्माण किया गया है।
2. स्थापत्य-संबंधी डिज़ाइनः
ऐसे समय में जब मंदिर प्राचीन ग्रंथों के आधार पर आयताकार बनाए जाते थे, होयसल मंदिर अपनी तारे के आकार/तारकीय योजनाओं, जटिल रूपों और उभरे हुए चबूतरों जैसी विशेषताओं के लिए जाने जाते थे।
स्थापत्य कला के विशिष्ट तत्वों जैसे कि खरादकर बनाए गए पत्थर के स्तंभ, घुमावदार और गोलाकार विमान या मंदिरों के ऊपर गुंबद और घंटी के आकार के कॉर्निस/छज्जे मंदिर स्थापत्य कला के विकास में महत्वपूर्ण नवाचार हैं। इसके अलावा, कल्याणी या सीढ़ीदार कुएं भी आम तौर पर पाए जाते हैं।
शहरों की योजना ब्रह्मांडीय आरेख पर बनाई गई थी जिसमें चार मुख्य दिशाओं में मुख्य अक्ष स्थापित किए गए थे और इन अक्षों के मिलन बिंदु अर्थात् चौराहे पर शहर के केंद्र में मुख्य मंदिर स्थापित किया गया था। मंदिर परिसर में विशाल रथों पर देवताओं की शोभायात्रा और परिक्रमा के लिए रथ बेदी अथवा चौड़ी सड़कें बनाई गई थीं।
3. सेलखड़ी का प्रयोगः
होयसल शासकों ने ग्रेनाइट के स्थान पर एक विशेष प्रकार के पत्थर का उपयोग किया जिसे लोकप्रिय रूप से सेलखड़ी (क्लोराइट शिस्ट) कहा जाता है।
स्थानीय रूप से पाया जाने वाला यह पत्थर उत्खनन के समय नर्म और लचीला होता है, लेकिन वायु के संपर्क में आने पर कठोर हो जाता है। इसलिए लगभग सभी होयसल मंदिरों में प्रचुर मात्रा में सुसज्जित प्रतिमाएं, अत्यधिक अलंकारिक उभरी आकृतियां और चित्र वल्लरियां पाई जाती हैं।
उदाहरण के लिए, बेलूर के चेन्नाकेशव मंदिर में 38 अद्भुत नक्काशीदार कोष्ठक के अंतर्गत आकृतियां निर्मित हैं जिन्हें शालभंजिका या मदनिका कहा जाता है।
4. एक से अधिक गर्भगृहः
होयसल मंदिरों को उनके गर्भगृहों की संख्या के आधार पर पांच प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है-
- एककुटा (एक गर्भगृह, जैसे- चेन्नाकेशव मंदिर),
- द्विकुटा (2 गर्भगृह; जैसे- होयसलेश्वर मंदिर),
- त्रिकुटा (3 गर्भगृह; जैसे- नरसिम्हा तृतीय द्वारा बनवाया गया सोमनाथपुर का केशव मंदिर),
- चतुष्कुटा (4 गर्भगृह; जैसे- लक्ष्मी देवी मंदिर, डोड्डागडुवल्ली) और
- पंचकुटा (5 गर्भगृह)।
निष्कर्ष:
होयसल मंदिर स्थापत्य कला में न केवल गहन अलंकृत नक्काशी में बल्कि भवन की संरचना और अखंडता में भी उत्कृष्ट विशेषज्ञता दिखाई देती है। अपनी विशिष्टता के कारण, हलेबिड्डु और बेलूर में होयसल के मंदिरों को यूनेस्को के तहत विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्रदान किया गया है।